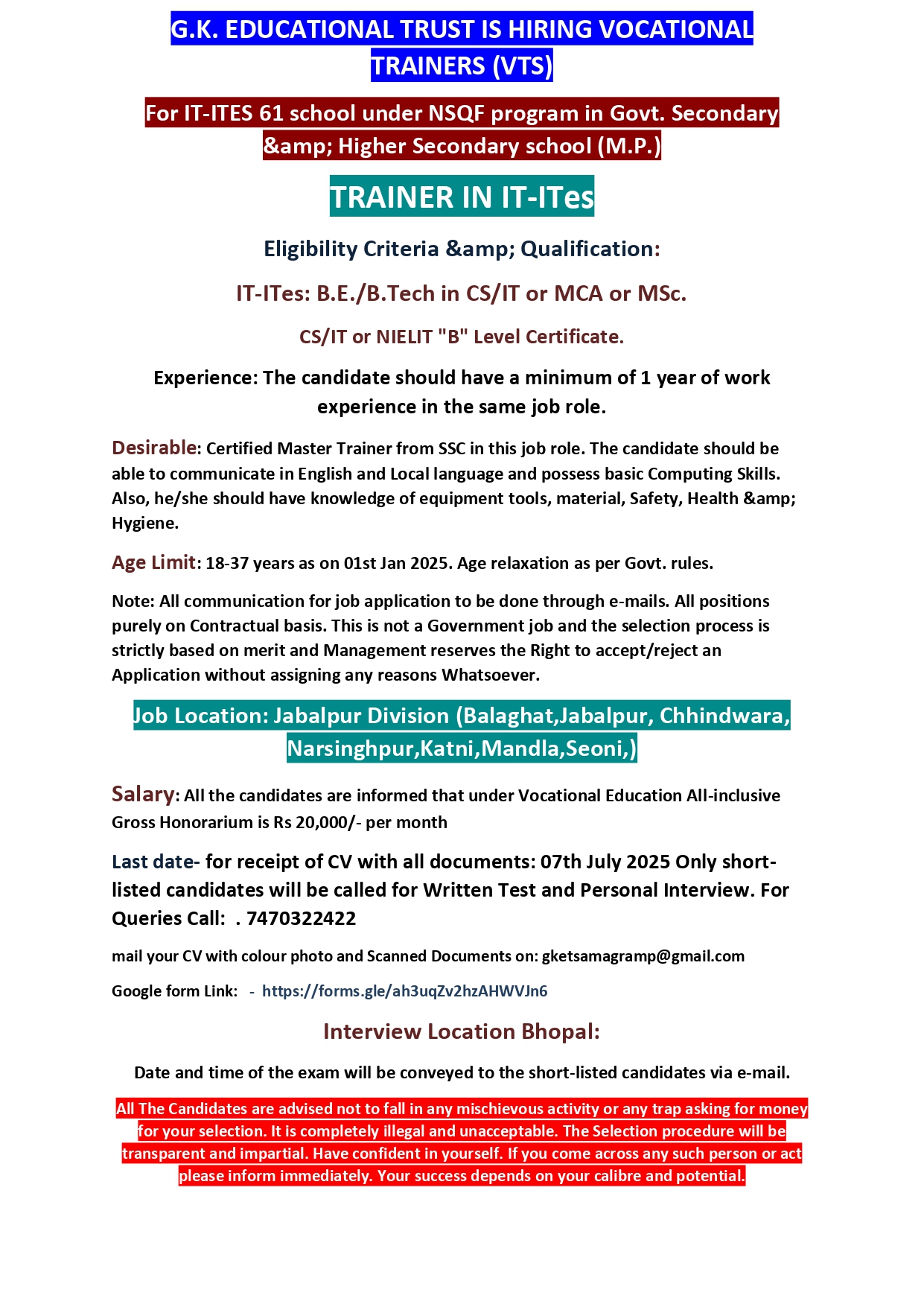आस्था की मलाई काटने के साथ धर्मगुरू लें पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी

भारत की 140 करोड़ आबादी का करीब एक तिहाई हिस्सा महाकुंभ के मेले में अपनी हाजिरी दर्ज करा चुका है. करीब छह हफ्ते का यह धार्मिक जमावड़ा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में लगा. राज्य सरकार के मुताबिक इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या सारे अनुमानों के पार चली गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह इस आयोजन की सारी तैयारी पर नजर रख रहे थे. उनका कहना है, "दुनिया भर में इंसानों के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव में करीब 52 करोड़ लोग आए यानी औसतन हर रोज करीब 1 करोड़ लोग."
गंदा पानी, कचरे का ढेर
हालांकि इस तरह के आयोजन पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियों को जन्म देते हैं. करोड़ों हिंदू तीर्थयात्रियों के यहां पहुंचने से स्थानीय जल संसाधन और इकोसिस्टमों पर भारी दबाव पड़ा है. इसके साथ ही भारी मात्रा में कचरा भी जमा हुआ है जिसमें ऐसी चीजें भी हैं जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होती और प्रदूषण का स्तर भी बड़ा है.
45 दिनों के इस धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार के दौरान गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता और कचरा प्रबंधन को लेकर चिंताएं बनी रही हैं.भारत के केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में गंगा और यमुना नदियों के संगम के पानी में फिकल कोलिफॉर्म के उच्च स्तर की रिपोर्ट दी थी. इसका मतलब है कि उस पानी में सीवेज की मात्रा मौजूद है.
जगद्गुरु कृपालु योग ट्रस्ट के आध्यात्मिक गुरु स्वामी मुकुंदानंद ने डीडब्ल्यू से कहा, "हमें प्रकृति को बचाने की जरूरत है, नहीं तो अगला कुंभ जब लगेगा तब गंगा या यमुना नहीं रहेंगी." यह ट्रस्ट समाज के विकास को बढ़ावा देता है. उन्होंने यह भी कहा, "यही वजह है कि हम लोगों को कचरा, सफाई, पर्यावरणऔर आरोग्य शास्त्र के बारे में सोचने और जागरुकता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं."
संत, धार्मिक और आध्यात्मिक नेता पहली बार कुंभ में साथ आ कर जलवायु संकट और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं और इनके समाधान में धार्मिक संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं.
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ध्यान दिलाया कि आस्था से जुड़े संगठन टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. वे अपनी प्रमुख सिद्धातों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से प्रेरित हैं.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने 2017 में द फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव शुरू किया था. यह रणनीतिक रूप से आस्था से जुड़े संगठनों को सतत विकास लक्ष्यों और 2030 के एजेंडे को हासिल करने के प्रयासों में शामिल करता है. इसी तरह इथियोपिया के ऑर्थोडॉक्स टेवाहेदो चर्च ने कई सदियों से जंगलों को बचाने में मदद दे कर जैव विविधता का संरक्षण किया है.
सिंह का कहना है, "हम लोग भी धर्मगुरुओं की मदद से लोगों को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. यह अभी शुरुआत है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है."ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख चिदानंद सरस्वती ने डीडब्ल्यू से कहा कि प्रकृति के लिए समर्पण और जिम्मेदारी को बढ़ावा दे कर आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ज्ञान और आधुनिक टिकाऊ जीवन के तौर तरीकों को जोड़ सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा, "अगर आस्था, धर्मगुरू, समाज और सरकार जुड़ जाएं तो हम समाधान निकाल सकते हैं."बहुत से लोगों का मानना है कि आस्था के जरिए शिक्षा और सक्रियता से धार्मिक नेता जलवायु के लिए किए जाने वाले कामों के अपने समुदायों में ताकतवर झंडाबरदार हो सकते हैं.
इंसानी गतिविधियों के कारण हो रहा जलवायु परिवर्तन पहले ही भारत में चरम मौसमी घटनाओं को जन्म दे रहा है. इसमें भयानक लू, बाढ़ और दूसरी आपदाएं शामिल हैं.इन घटनाओं ने भोजन, पानी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है. पुण के इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी में जलवायु विज्ञानी रॉक्सी मैथ्यू कॉल का कहना है, "ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा इलाका गर्म हवाओं, बाढ़, भूस्खलन, सूखा और आंधियों के एक ट्रेंड को देख रहा है."
इंटरनेशनल फोरम फॉर इनवायरनमेंट, सस्टेनिबिलिटी एंट टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्र भूषण का कहना है कि वैज्ञानिक समुदायों और सरकारी अधिकारियों ने यह मोटे तौर पर मान लिया है कि उनकी पहुंच सीमित है.
"सिर्फ वैज्ञानिक जानकारियां देना लोगों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. वे जलवायु परिवर्तन और उसके असर को तब समझते हैं जब वे उसे अपने जीवन से जोड़ कर देख पाते हैं. विज्ञान और सरकारी कार्यक्रम यह करने में असमर्थ हैं."
उन्होंने यह भी कहा कि धर्मगुरु इस खाई को भरने में मदद कर सकते हैं. वे समुदायों को आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर अपने साथ जोड़ कर, "टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा और नीतियों में बदलाव की पैरवी" कर सकते हैं.
संयुक्त राष्ट्र की इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की है. इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि देश आने वाले दो दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली कई आपदाओं का सामना कर सकता है.
धार्मिक नेताओं ने अपने अनुयायियों में पर्यावरण अनुकूल तौर तरीकों को बढ़ावा देने का वचन दिया है. इसमें अक्षय ऊर्जा को अपनाना, कचरे के प्रबंधन की नीतियों को लागू करना और आस्थावान समुदायों में जलवायु शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ाना शामिल है.
गैर सरकारी संगठन श्रीराम चंद्र मिशन की शालिनी मल्होत्रा ने डीडब्ल्यू से कहा, "हमने यह संदेश फैलाने के लिए कोशिशें की हैं. आइए यह उम्मीद करें कि आध्यामिक और धार्मिक नेताओं का यह जमावड़ा टिकाऊ तरीकों को अपनाने के मिशन को जिंदा रखेगा.

 जानें, मंगलसूत्र धारण करने के नियम और इसका महत्व
जानें, मंगलसूत्र धारण करने के नियम और इसका महत्व राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन ( 03 जुलाई 2025)
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन ( 03 जुलाई 2025) पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रीता बनाफर ने पर्यावरण संरक्षण में दिया योगदान, बिजली बिल में भी मिली राहत
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रीता बनाफर ने पर्यावरण संरक्षण में दिया योगदान, बिजली बिल में भी मिली राहत पैरा खिलाड़ी तिवारी की राह हुई आसान
पैरा खिलाड़ी तिवारी की राह हुई आसान नागौद सब-स्टेशन में अब डबल एक्स्ट्रा हाईटेंशन सप्लाई की सुविधा
नागौद सब-स्टेशन में अब डबल एक्स्ट्रा हाईटेंशन सप्लाई की सुविधा